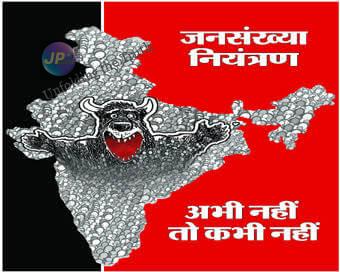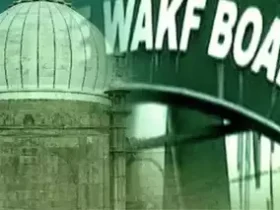गोपनीयता और सुरक्षा चिंताओं के बारे में हालिया विवादों ने निजता के अधिकार से संबंधित मुद्दों पर बहस को सबसे आगे ला दिया है। जबकि भारत के संविधान, 1950 ने स्पष्ट रूप से निजता के मौलिक अधिकार को प्रदान नहीं किया, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ में इस अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत पढ़ा। भले ही निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों के ढांचे में हाल ही में लाया गया था, क्या भारतीय संवैधानिक इतिहास में इस अधिकार की मांग थी?
उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, गोपनीयता का विचार घर या संपत्ति की हिंसा के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। भारत का संविधान विधेयक 1895, भारत के लिए एक संवैधानिक कल्पना को पेश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, जिसमें कहा गया है: ‘प्रत्येक नागरिक के घर में एक अदृश्य शरण है।’ इसके बाद, भारत के राष्ट्रमंडल विधेयक, 1925 ने बिना किसी उचित प्रक्रिया के आवास में अनुचित हस्तक्षेप की रक्षा की। सर्वदलीय सम्मेलन के परिणाम अधिवक्ता मोतीलाल नेहरू ने 1928 में समान अधिकार की गारंटी दी।
औपचारिक संविधान-निर्माण की शुरुआत से कुछ साल पहले, फ्री इंडिया का संविधान: ए ड्राफ्ट (एम.एन. रॉय, 1944), जैसा कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा समर्थन किया गया था, पहली बार निजी पत्र-व्यवहार को शामिल करने के लिए संपत्ति से परे निजता के अधिकार को बढ़ाया गया था। चार साल बाद भारतीय गणराज्य (सोशलिस्ट पार्टी, 1948) के संविधान के मसौदे ने कानून की उचित प्रक्रिया को छोड़कर किसी के घर में गैरकानूनी प्रवेश के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की।
गोपनीयता और संविधान सभा-
संविधान सभा ने औपचारिक रूप से दिसंबर 1946 में संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। इसने रिपोर्ट तैयार करने के लिए कई समितियों का गठन किया, जिसके आधार पर मसौदा समिति एक मसौदा संविधान विकसित करेगी।
समिति के चरणों में, मौलिक अधिकारों पर उप-समिति के सदस्यों के एक समूह ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की वकालत की। केएम मुंशी ने अपने घर की हिंसा के अधिकार और किसी के पत्राचार की गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की मांग की। डॉ बीआर अंबेडकर ने अपने राज्यों और अल्पसंख्यक रिपोर्ट में ‘लोगों के अपने व्यक्तियों, घरों, कागजात और अनुचित खोजों और जब्ती के खिलाफ प्रभाव’ में सुरक्षित होने के अधिकार की वकालत की।
इन सभी प्रस्तावों का जोरदार विरोध हुआ। बीएन राव (संविधान सभा के सलाहकार) और संविधान सभा के सदस्य अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर मौलिक अधिकारों के भीतर निजता के अधिकार को शामिल करने से असहमत थे। बीएन राव मुख्य रूप से पुलिस अधिकारियों की जांच शक्तियों के साथ निजता के अधिकार के हस्तक्षेप से चिंतित थे। जबकि अय्यर का मानना था कि पत्राचार में गोपनीयता और गोपनीयता का अधिकार देना विनाशकारी होगा: यह प्रत्येक निजी/नागरिक संचार को राज्य के कागजात के स्तर तक बढ़ा देगा। यह नागरिक मुकदमेबाजी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जहां दस्तावेज साक्ष्य का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।
बीएन राव और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर दोनों ही सलाहकार समिति को निजता के अधिकार से संबंधित प्रावधानों को छोड़ने के लिए राजी करने में सफल रहे। सलाहकार समिति की अंतिम रिपोर्ट में निजता के अधिकार का कोई उल्लेख नहीं था।
संविधान सभा के पूर्ण सत्र में, मौलिक अधिकार अध्याय में निजता के अधिकार के प्रावधानों को पेश करने के दो अलग-अलग प्रयास मिल सकते हैं।
30 अप्रैल 1947 को, सोमनाथ लाहिड़ी ने पत्राचार के निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि, उनके प्रस्ताव को कोई कर्षण नहीं मिला। एक साल बाद काजी सैयद करीमुद्दीन ने संविधान के अनुच्छेद 20 (मसौदा अनुच्छेद 14) में अनुचित खोजों और जब्ती के खिलाफ लोगों के अपने व्यक्तियों, घरों, कागजात और प्रभावों में सुरक्षित होने के अधिकार को शामिल करने के लिए स्थानांतरित किया। उन्होंने अमेरिकी और आयरिश संविधान के उदाहरणों का हवाला दिया और अम्बेडकर के मौलिक अधिकारों की उप-समिति को इसी तरह के प्रस्ताव की विधानसभा को याद दिलाया। सैयद करीमुद्दीन को मनमानी खोजों से मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भी प्रेरित किया गया था। उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद पूर्वाग्रहों में घिरी राज्य एजेंसियों ने मुसलमानों के साथ ‘अपराधियों’ जैसा व्यवहार किया। यह संशोधन विधानसभा में पराजित हो गया था।
निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाने के पिछले सभी प्रयास विफल रहे थे।
कई मामलों के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1954 में एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्र, वर्ष 1962 खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, वर्ष 1975 गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य और वर्ष 2017 न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ में अपने निर्णय में इस पर व्याख्या की-
वर्ष 1954
एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्र-
यह मामला डालमिया समूह की कुछ कंपनियों के मामलों की जांच के बाद उनके दस्तावेजों की तलाशी और जब्ती से संबंधित है। एक प्राथमिकी के बाद, जिला मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया, और परिणामस्वरूप तलाशी ली गई। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिकाओं में, खोजों की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उन्होंने अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और 20 (3) के तहत अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया – आत्म-अपराध के खिलाफ सुरक्षा। एम. पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट की 8 जजों की बेंच ने माना कि संविधान के मसौदे का इरादा तलाशी और जब्ती की शक्ति को निजता के मौलिक अधिकार के अधीन करने का नहीं था। उन्होंने कहा कि संविधान में अमेरिकी संविधान के चौथे संशोधन के समान भाषा शामिल नहीं है, और खोज-और-जब्ती में गोपनीयता के मौलिक अधिकार की अवधारणा को आयात करने का कोई औचित्य नहीं मिला, जिसे उन्होंने ‘तनावपूर्ण निर्माण’ कहा।
वर्ष 1962
खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य-
पुलिस द्वारा एक आरोपी व्यक्ति की निगरानी को चुनौती देने के लिए इस मामले में निजता का अधिकार लागू किया गया था। खड़क सिंह को डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया गया था लेकिन सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाद में उसे निगरानी में लाया, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अध्याय XX के तहत अनुमति दी गई थी। खड़क सिंह ने तब अध्याय XX की संवैधानिक वैधता और पुलिस अधिकारियों को दी गई शक्तियों को चुनौती दी, क्योंकि इसने अनुच्छेद 19 (1) (डी) (आंदोलन की स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत की सुरक्षा) के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया। स्वतंत्रता)। 6-न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि रात में अधिवास का दौरा असंवैधानिक था, लेकिन बाकी विनियमों को बरकरार रखा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकार नहीं है।
वर्ष 1975
गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य-
गोविंद ने खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के समान अधिवास यात्राओं सहित निगरानी से संबंधित मध्य प्रदेश पुलिस विनियमों की वैधता को चुनौती दी। गोविंद ने उन पर झूठे आरोप लगाए जिसके आधार पर उन्हें पुलिस ने निगरानी में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस के नियमों में सुधार की सलाह दी और कहा कि वे ‘असंवैधानिकता के करीब खतरनाक’ थे।
वर्ष 2017
न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ-
24 अगस्त 2017 को, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ और अन्य जुड़े मामले, इस बात की पुष्टि करते हुए कि भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को निजता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। हालांकि सर्वसम्मत, फैसले में 6 अलग-अलग सहमति वाले फैसले देखे गए। चंद्रचूड़ जे ने अपने लिए बोलते हुए निर्णय लिखा, खेहर और आर.के. अग्रवाल और अब्दुल नज़ीर जे. शेष 5 न्यायाधीशों ने प्रत्येक ने व्यक्तिगत सहमति वाले निर्णय लिखे
वर्ष 2017 में, अंततः निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग घोषित किया।
लेखक – अमृतेष कुमार मृत्युंजय