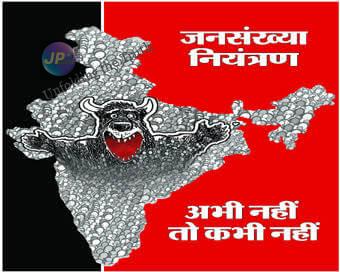कुछ और कहने से पहले यह उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अभियोजन पक्ष जिस अपमानजनक तरीके से यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित एफआईआर से निपटने के लिए समय सीमा के विस्तार के लिए एक आवेदन दायर करने में विफल रहा, उसकी आलोचना करते हुए स्वयंभू के खिलाफ गॉडमैन शिव शंकर बाबा, मद्रास उच्च न्यायालय ने 2021 के Crl.O.P.No.23806 और Crl.M.P. 2021 की संख्या 13107, जिसे 29 नवंबर, 2022 को आरक्षित किया गया था और फिर 1 मार्च, 2023 को अंतिम रूप से घोषित किया गया था, ने ऐसे मामलों में सीमा के विस्तार के संबंध में कई दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।
याचिका में की गई प्रार्थना पर विचार करते हुए, खंडपीठ ने निर्दिष्ट किया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई आपराधिक मूल याचिका, जिसमें प्रथम प्रतिवादी पुलिस निरीक्षक द्वारा दर्ज 2021 के अपराध संख्या 2 से संबंधित रिकॉर्ड की मांग करने की प्रार्थना की गई है। , CBCID, OCU पुलिस स्टेशन-II, चेन्नई और याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करें।
यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि न्यायमूर्ति आरएन मंजुला की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने बाबा द्वारा दायर याचिका का निस्तारण किया था, यह देखते हुए कि वास्तविक शिकायतकर्ता ने विचारण द्वारा संज्ञान के आदेश को रद्द करने के लिए एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। अदालत।
निस्संदेह, अभियोजन एजेंसी को सभी संभव कार्रवाई करनी चाहिए थी और अदालतों को देरी को माफ करने या समय सीमा के विस्तार के लिए याचिका को खारिज करने का निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए था। मौजूदा मामले में अभियोजन पक्ष और अदालत दोनों ही ऐसा करने में विफल रहे हैं। इस सब के कारण आपराधिक मामलों में सीमा अवधि बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश जारी करना और भी आवश्यक हो गया था जो तदनुसार किया गया है!
सर्वप्रथम, माननीय जस्टिस आरएन मंजुला की मद्रास उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश खंडपीठ द्वारा लिखित इस संक्षिप्त, शानदार, साहसिक और संतुलित निर्णय ने सबसे पहले पैरा 1 में यह बताते हुए गेंद को गति प्रदान की कि, “यह आपराधिक मूल याचिका प्रथम प्रतिवादी पुलिस की फ़ाइल पर 2021 के अपराध संख्या 2 से संबंधित रिकॉर्ड की मांग करने और उसी को रद्द करने के लिए दायर की गई है।”
चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, खंडपीठ ने पैरा 2 में परिकल्पना की है कि, “2021 के अपराध संख्या 2 में मामला याचिकाकर्ता के खिलाफ शैक्षणिक वर्ष 2010-2011 के बीच दूसरे प्रतिवादी के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर दर्ज किया गया है। दूसरे प्रतिवादी ने 20.07.2021 को ई-मेल के माध्यम से शिकायत भेजी और एफ.आई.आर. उसी के आधार पर आईपीसी की धारा 354 और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।”
कहने की जरूरत नहीं है कि खंडपीठ ने पैरा 3 में कहा है कि, “इस याचिका के तथ्यों और योग्यताओं पर ध्यान देने से पहले, उस प्रक्षेपवक्र का उल्लेख करने की आवश्यकता है जिसके कारण आदेश के इस चरण तक पहुंचा। दिनांक 17.10.2022 के पूर्व आदेश के आधार पर, यह आपराधिक मूल याचिका निस्तारित हो गई। यह आदेश प्राथमिकी को रद्द करने के प्रभाव का था। धारा 468 Cr.P.C के तहत सीमा के आधार पर याचिका की अनुमति देकर।”
इसके अलावा, खंडपीठ ने पैरा 4 में स्पष्ट किया कि, “बाद में दूसरी प्रतिवादी ने यह कहते हुए आदेश को वापस लेने के लिए एक याचिका दायर की है कि उसे आपराधिक मूल याचिका का निपटान करने से पहले नोटिस नहीं दिया गया है। हालांकि पहले प्रतिवादी/राज्य को विस्तार से सुना गया था, राज्य ने भी दूसरे प्रतिवादी द्वारा बताए गए कारणों को बताते हुए एक ही प्रार्थना की मांग करते हुए एक अलग याचिका दायर की थी।
उन याचिकाओं को 2022 के Crl.M.P.Nos.16421 और 16422 में निपटाया गया है। उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, पहले प्रतिवादी ने कहा कि चार्जशीट दायर की जा चुकी है और इसे सी.सी. में ट्रायल कोर्ट द्वारा फाइल पर ले लिया गया है। 2022 की संख्या 654, यहां तक कि जब आपराधिक मूल याचिका पर सुनवाई हुई थी और इसलिए आपराधिक मूल याचिका को निष्फल मानकर खारिज कर दिया जाना चाहिए था।”
ध्यान दें, खंडपीठ पैरा 24 में बताती है कि, “उपरोक्त फैसले का समग्र अध्ययन यह दिखाएगा कि देरी को माफ करने के लिए याचिका दायर करने के संबंध में प्रक्रियात्मक छूट विशुद्ध रूप से न्याय के हित पर आधारित है।
JOSEPH बनाम केरल राज्य में (1989) 2 केरल में रिपोर्ट किया गया। एलटी 710, यह देखा गया है कि 6 वर्ष या 9½ वर्ष जैसे अत्यधिक विलंब को माफ करके अभियोजन को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।
एआईआर 1995 एससी 231 में रिपोर्ट किए गए महाराष्ट्र राज्य बनाम एस.वी. डोंगरे में, यह माना जाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा देरी को माफ करने के लिए दिए गए आवेदन में, विपरीत पक्ष को अवसर की सूचना दी जानी चाहिए। आरोपी को उचित नोटिस दिए बिना विलंब को माफ करने के आदेश को उचित नहीं ठहराया गया।”
प्रासंगिक मामले कानून का उल्लेख करते हुए, खंडपीठ ने पैरा 25 में कहा है कि, “सुखदेव राज बनाम पंजाब राज्य में 1994 एससीसी (सीआरआई) 1480 में भी रिपोर्ट किया गया था, यह दावा किया जाता है कि धारा 473 सीआरपीसी। यह निर्धारित नहीं करता है कि देरी को क्षमा करने के लिए आवेदन चालान दाखिल करने के समय ही दायर किया जाना चाहिए और न्यायालय देरी को माफ कर सकता है यदि इसे ठीक से समझाया गया है और न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है।”
यह उल्लेख करना उचित होगा कि खंडपीठ ने पैरा 26 में कहा है कि, “जैसा कि धारा 468 सीआरपीसी के प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है, सीमा का प्रश्न केवल उन अपराधों के लिए लागू होता है जो तीन से अधिक अवधि के लिए दंडनीय नहीं हैं। वर्षों का कारावास। हालांकि धारा 473 Cr.P.C के तहत सीमा की अवधि को बढ़ाने के लिए न्यायालय को विवेक प्रदान किया गया है। इसे न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए और आदेश न्यायालय की संतुष्टि को इंगित करते हुए एक स्पष्ट आदेश के माध्यम से होना चाहिए कि देरी को संतोषजनक ढंग से समझाया गया था और उसी की क्षमा न्याय के हित में थी।
यह हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम तारा दत्त में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले में आयोजित किया गया है (2000) 1 एससीसी 230 में बताया गया है कि उस प्रभाव के किसी भी सकारात्मक आदेश के अभाव में यह स्वीकार्य नहीं है उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि न्यायालय ने देरी को माफ करके संज्ञान लिया था। शिखिल कटोच बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में 2020 एससीसी ऑनलाइन एचपी 2693 में रिपोर्ट की गई, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने उपरोक्त सिद्धांत का पालन किया है और निम्नानुसार आयोजित किया है: –
“17। ….. धारा 473 Cr.P.C. सीमा की अवधि की समाप्ति के बाद न्यायालय को संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करता है, यदि उसमें परिकल्पित शर्तों को पूरा किया जाता है, अर्थात जहां देरी का उचित और संतोषजनक स्पष्टीकरण उपलब्ध है और जहां न्यायालय संज्ञान लेता है कि यह न्याय के हित में होगा , और न्यायालय को प्रदत्त इस विवेकाधिकार का न्यायिक रूप से और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों पर प्रयोग किया जाना चाहिए और जहां भी न्यायालय इस विवेक का प्रयोग करता है, वही एक स्पष्ट आदेश द्वारा होना चाहिए, संतोषजनक स्पष्टीकरण और हित के संबंध में न्यायालय की संतुष्टि का संकेत देना चाहिए न्याय।
यह भी देखा गया है कि इस आशय के सकारात्मक आदेश के अभाव में, उच्च न्यायालय के लिए इस निष्कर्ष पर आने की अनुमति नहीं हो सकती है कि जब भी संज्ञान पर रोक लगाई गई थी और तब भी न्यायालय ने विलंब को माफ करके संज्ञान लिया हो, ऐसा माना जाना चाहिए। न्यायालय ने संज्ञान लिया और अपराध के विचारण के साथ आगे बढ़ा और समाज को प्रभावित करने वाले अपराध का संज्ञान लेने के मामले में, मजिस्ट्रेट को उदारतापूर्वक परिसीमन के प्रश्न का अर्थ निकालना चाहिए, लेकिन मामले की जिन परिस्थितियों में देरी की आवश्यकता होती है, उन्हें प्रकट होना चाहिए। मजिस्ट्रेट का ही आदेश।
प्रासंगिक विचार पर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग किए गए विवेक को दोष नहीं दिया जा सकता है।
सबसे उल्लेखनीय रूप से, खंडपीठ ने पैरा 28 में कहा है कि, “जहां तक निजी शिकायत प्रक्रिया को अपनाकर दर्ज की गई शिकायतों का संबंध है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि शिकायतकर्ता को अपराध वर्जित होने की स्थिति में देरी को माफ करने के लिए याचिका दायर करनी होगी।” उस समय परिसीमन द्वारा जब शिकायत दर्ज की गई थी और जिस पर अभियुक्त को अवसर का नोटिस देने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा एक आदेश पारित किया जाना था।
“दंड प्रक्रिया संहिता में अध्याय XXXVI लाने के लिए (2014) 2 एससीसी 62 में रिपोर्ट किए गए सारा मैथ्यू बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो वैस्कुलर डिजीज में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण अवलोकन को दोहराना सार्थक है। उक्त निर्णय में, विधि आयोग की रिपोर्ट और संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बारे में एक संदर्भ दिया गया है जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता में अध्याय XXXVI को सम्मिलित करने के उद्देश्य का उल्लेख किया गया है। महत्वपूर्ण पैराग्राफ नं। उपरोक्त विषय पर 17 से 20 निम्नानुसार निकाले जाते हैं:-
“17। संयुक्त संसद समिति (“जेपीसी”) ने कुछ अपराधों के लिए परिसीमा अवधि निर्धारित करने के लिए विधि आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया। इसकी रिपोर्ट के संबंधित पैराग्राफ दिनांक 30/11/1972 को निम्नानुसार पढ़ा गया:
“खंड 467 से 473 (नए खंड) – ये कुछ मामलों में आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए एक श्रेणीबद्ध पैमाने पर सीमा की अवधि निर्धारित करने वाले नए खंड हैं। वर्तमान में, आपराधिक अभियोजन के लिए कोई सीमा अवधि नहीं है और एक अदालत केवल देरी के आधार पर शिकायत या पुलिस रिपोर्ट को खारिज नहीं कर सकती है, हालांकि अभियोजन पक्ष की कहानी की सच्चाई के बारे में संदेह पैदा करने के लिए असामान्य देरी एक अच्छा आधार हो सकती है। कई देशों के कानूनों में आपराधिक अभियोजन के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है और समिति महसूस करती है कि कानून आयोग द्वारा अनुशंसित संहिता में ऐसी अवधि निर्धारित करना वांछनीय होगा।
सीमा निर्धारित करने के पक्ष में निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया जा सकता है-
- जैसे-जैसे समय बीतता है गवाहों की गवाही कमजोर और कमजोर होती जाती है क्योंकि याददाश्त कमजोर हो जाती है और सबूत अधिक से अधिक अनिश्चित हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप त्रुटि का खतरा अधिक हो जाता है।
- शांति और विश्राम के उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि एक अपराधी को लगातार इस आशंका के तहत नहीं रखा जाना चाहिए कि उस पर किसी भी समय मुकदमा चलाया जा सकता है, विशेष रूप से क्योंकि विविध कानूनों के कारण नए अपराध पैदा होते हैं, एक समय में कई व्यक्ति कुछ अपराध करते हैं। या अन्य। लोगों के मन में शांति नहीं होगी यदि छोटे-मोटे अपराधों के लिए भी समय सीमा न हो।
- यदि अभियोजन शुरू नहीं किया जाता है और अपराध से संबंधित व्यक्तियों की स्मृति को मिटा दिए जाने से पहले सजा नहीं दी जाती है, तो सजा का निवारक प्रभाव बिगड़ा हुआ है।
- सामाजिक प्रतिशोध की भावना जो आपराधिक कानून के उद्देश्यों में से एक है, एक लंबी अवधि की समाप्ति के बाद अपनी धार खो देती है।
- सीमा की अवधि आपराधिक अभियोजन के अंगों पर अपराध का जल्द से जल्द पता लगाने और सजा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का दबाव बनाएगी। समिति की राय में, अपराधों की गंभीरता और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, नए खंडों में प्रदान की गई समय सीमा की वास्तविक अवधि उपयुक्त होगी।
जिस तिथि से अवधि की गणना की जानी है, उस तिथि के संबंध में विचार की गई समिति ने तिथि को अपराध की तिथि के रूप में निर्धारित किया है। हालाँकि, इससे व्यावहारिक कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं और एक अभियुक्त व्यक्ति को निर्धारित अवधि के लिए केवल खुद को फरार होने से सजा से बचने में मदद मिल सकती है, समिति ने यह भी प्रावधान किया है कि जब अपराध से पीड़ित व्यक्ति को अपराध का पता नहीं था या किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए, सीमा की अवधि उस दिन से शुरू होगी जिस दिन अपराध में अपराधी की भागीदारी के बारे में सबसे पहले अपराध से पीड़ित व्यक्ति या किसी पुलिस अधिकारी की जानकारी में आता है, जो भी पहले हो,”।
“इसके अलावा, जब यह ज्ञात नहीं है कि अपराध किसके द्वारा किया गया है, तो पहले दिन जिस दिन अपराधी की पहचान अपराध से पीड़ित व्यक्ति या अपराध की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को पता चलती है। समिति ने समय के विस्तार के लिए एक विशिष्ट प्रावधान करना आवश्यक माना है जब भी अदालत सामग्री पर संतुष्ट हो कि देरी को ठीक से समझाया गया है या आरोपी फरार हो गया है। यह प्रावधान विशेष रूप से उपयोगी होगा क्योंकि इस देश में पहली बार आपराधिक मुकदमा चलाने की सीमा निर्धारित की जा रही है।
- विधि आयोग की रिपोर्ट और जेपीसी की रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में पढ़ें, यह स्पष्ट है कि अध्याय XXXVI का उद्देश्य Cr.P.C में डाला गया है। शिकायतों के अभियोगों को तेज करना और अत्यधिक सुस्ती, जड़ता या आलस्य प्रदर्शित करने वाले अप्रासंगिक मामलों की आपराधिक न्याय प्रणाली से छुटकारा पाना था। कुछ अपराधों के लिए परिसीमा अवधि प्रदान करके आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक व्यवस्थित, कुशल और न्यायपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया था। सरवन सिंह मामले में, इस न्यायालय ने परिसीमा की रोक लगाने में Cr.P.C की वस्तु को इस प्रकार बताया:
“अभियोजन पर परिसीमन की रोक लगाने में आपराधिक प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य स्पष्ट रूप से पक्षकारों को लंबे समय के बाद मामले दर्ज करने से रोकना था, जिसके परिणामस्वरूप भौतिक साक्ष्य गायब हो सकते हैं और अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को भी रोका जा सकता है। अपराध की तारीख के लंबे समय बाद तंग करने वाला और विलंबित मुकदमा दायर करके। जिस वस्तु को कानून उप-सेवा करना चाहते हैं वह स्पष्ट रूप से परीक्षण की निष्पक्षता की अवधारणा के अनुरूप है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। इसलिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कोई भी अभियोजन, चाहे राज्य द्वारा या एक निजी शिकायतकर्ता द्वारा कानून के पत्र का पालन करना चाहिए या परिसीमा के आधार पर अभियोजन पक्ष के विफल होने का जोखिम उठाना चाहिए।
- हालांकि यह समान रूप से स्पष्ट है कि कानून निर्माता नहीं चाहते थे कि वास्तविक मामलों में न्याय का नुकसान हो। विधि आयोग ने समय के अपवर्जन के प्रावधानों की सिफारिश की और उन प्रावधानों को अध्याय XXXVI का हिस्सा बनाया गया। इसलिए, हम अध्याय XXXVI में कुछ मामलों (धारा 470) में समय के अपवर्जन के लिए, उस तारीख के बहिष्करण के लिए जिस पर न्यायालय बंद है (धारा 471), निरंतर अपराधों के लिए (धारा 472) और परिसीमा की अवधि के विस्तार के लिए प्रावधान पाते हैं। कुछ मामलों में (धारा 473)। धारा 473 महत्वपूर्ण है। यह न्यायालय को परिसीमा की अवधि की समाप्ति के बाद किसी अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देता है, यदि वह तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में संतुष्ट है कि देरी को उचित रूप से समझाया गया है या ऐसा करना आवश्यक है न्याय हित. इसलिए, शिकायतकर्ता के खिलाफ अध्याय XXXVI लोड नहीं किया गया है। यह सच है कि आरोपी को त्वरित सुनवाई का अधिकार है और यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक पहलू है।
“Cr.P.C का अध्याय XXXVI। अभियुक्त के इस अधिकार को कम नहीं करता है। हालांकि यह परिसीमा प्रदान करके परिश्रम को प्रोत्साहित करता है, लेकिन यह नहीं चाहता कि सभी मुकदमों को देरी के आधार पर खत्म कर दिया जाए। यह शिकायतकर्ता के हित और अभियुक्त के हित के बीच संतुलन बनाता है।
“यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि जहां विधायिका कुछ अपराधों को अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती थी, उसने धारा में ही सीमा के लिए प्रावधान किया, उदाहरण के लिए, Cr.P.C की धारा 198(6) और 199(5)। हालाँकि, इसने पहली बार कुछ प्रकार के अपराधों के लिए परिसीमन के लिए सामान्य प्रावधान बनाने का विकल्प चुना और उन्हें Cr.P.C के अध्याय XXXVI में शामिल किया।
सबसे सराहनीय बात यह है कि खंडपीठ ने पैरा 29 में कहा है कि, “पंजाब राज्य बनाम. सरवन सिंह ने 1981 स्केल (1) 619 में बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सीमा के कारण रोक लगाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित मुकदमे की निष्पक्षता की अवधारणा के अनुरूप है।
“यह आगे माना जाता है कि अध्याय XXXVI के लिए अत्यधिक महत्व का पालन किया जाना चाहिए और कानून के पत्र में, किसी भी अभियोजन पक्ष में, चाहे राज्य या निजी शिकायतकर्ता द्वारा,”।
“या फिर, इसे सीमा के आधार पर अभियोजन पक्ष के विफल होने का जोखिम उठाना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि अध्याय XXXVI शिकायतकर्ता के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित परीक्षण के अधिकार और पीड़ित के लिए न्याय पाने के अधिकार के बीच एक संतुलन है जो किसी अपराध के कमीशन के कारण प्रभावित होता है।
खंडपीठ ने पैरा 51 में कहा है कि, “यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि त्वरित सुनवाई निष्पक्ष सुनवाई के लिए मूल तत्व है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का एक पहलू है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। यदि एक पुलिस अधिकारी एक मामला दर्ज करता है जिसमें उस समय सीमा द्वारा वर्जित अपराध शामिल होता है जब यह दर्ज किया गया था और आरोपी की जांच या गिरफ्तारी भी करता है, तो यह उसकी निरंकुश शक्तियों के कारण हो सकता है, “।
“लेकिन न्यायालय इसका समर्थन नहीं कर सकता, जब तक कि यह न्याय के हित में नहीं दिखाया जाता है। फिर भी, न्यायालय विरोधी पक्ष को अवसर का कोई नोटिस दिए बिना और धारा 473 Cr.P.C के तहत सीमा के विस्तार के लिए एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किए बिना एक समय-बाधित शिकायत पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है।”
इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि खंडपीठ पैरा 58 में बताती है कि, “मामले में, हालांकि यह पहले प्रतिवादी / राज्य द्वारा दायर काउंटर में कहा गया है कि वे धारा 473 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर करेंगे। सीमा को बढ़ाने या माफ करने के लिए, चार्जशीट दाखिल करते समय, पहले प्रतिवादी ने सीआरपीसी की धारा 473 के तहत ऐसी कोई याचिका दायर नहीं की थी।”
“एक तरफ, अभियोजन पक्ष जोरदार तरीके से यौन अपराधों की गंभीरता के बारे में तर्क देता है, लेकिन दूसरी तरफ यह धारा 473 Cr.P.C के तहत याचिका दायर नहीं करने के लिए उदासीन रहता है। उस समय जब आरोप पत्र दायर किया गया था और इस प्रकार अभियुक्तों के लिए यह दावा करने के लिए आधार तैयार किया गया था कि दायर की गई आरोप पत्र कानूनी रूप से गैर-स्थायी है।
“न्यायालय से गंभीर विचार की मांग करने वाली अभियोजन एजेंसी को भी जल्द से जल्द हर संभव कार्रवाई करके गंभीर तरीके से काम करना चाहिए था।”
काफी महत्वपूर्ण रूप से, खंडपीठ ने पैरा 59 में यह कहते हुए जल्दबाजी की कि, “दोहराव के जोखिम पर, यह दोहराया जाता है कि अध्याय XXXVI को शुरू करने का उद्देश्य पार्टियों को लंबे समय के बाद मामले दर्ज करने से रोकना है और जिसके परिणामस्वरूप भौतिक साक्ष्य गायब हो सकते हैं और लंबे समय के बाद कष्टप्रद और विलंबित अभियोजन दायर करके न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। जैसा कि पंजाब राज्य बनाम सरवन सिंह के मामले में 1981 स्केल (1) 619 में रिपोर्ट किया गया था कि कोई भी अभियोजन चाहे राज्य द्वारा या एक निजी शिकायतकर्ता के माध्यम से, कानून के पत्र का पालन करना चाहिए या अभियोजन पक्ष के विफल होने का जोखिम उठाना चाहिए सीमा का आधार, ”।
“ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही अभियुक्त को परिसीमा द्वारा वर्जित मामले में दोषी ठहराया गया हो, पूरी कार्यवाही दूषित हो जाएगी और गैर-स्थायी हो जाएगी,”।
“विलंब को क्षमा करते हुए भी, न्याय के हित को सर्वोपरि भूमिका निभानी है और कोई अन्य असाधारण कारण नहीं हैं। इसलिए अदालत को अपराध की प्रकृति, पीड़िता किस वर्ग की है और पीड़िता की पृष्ठभूमि, आरोपी द्वारा पीड़िता द्वारा की गई क्रूरता या अमानवीय व्यवहार आदि पर ध्यान देना होगा।
“देरी माफ करने के अनुरोध पर विचार करते हुए। अपराध की असंगत प्रकृति, अभियोजन पक्ष की ओर से जानबूझकर निष्क्रियता आदि जैसे कोई भी कारक, न्याय के हित को विफल कर देंगे और इसलिए समय सीमा के विस्तार के लिए याचिका को खारिज करने के कारण हो सकते हैं।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि खंडपीठ ने पैरा 60 में नोट किया कि, “मामले में, माना जाता है कि न तो अभियोजन पक्ष ने देरी को माफ करने के लिए कोई याचिका दायर की थी और न ही क्षेत्राधिकार न्यायालय ने कोई स्पष्ट आदेश पारित किया है कि मामले का संज्ञान क्यों लिया गया है हालांकि अपराध सीमा से वर्जित है और उस समय दस साल की देरी थी जब एफ.आई.आर. पंजीकृत किया गया था।”
जैसा कि हम देखते हैं, खंडपीठ पैरा 61 में कहती है कि, “याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि संज्ञान उस मामले में लिया गया था जो घटना की तारीख से दस साल की देरी के कारण पहले से ही सीमित है, कार्यवाही कानून की नजर में गैर-स्थायी हो गई है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खंडपीठ ने पैरा 63 में आदेश देने के लिए कोई शब्द नहीं दिया है कि, “आपराधिक मामलों पर लागू सीमा के कानून पर उपरोक्त चर्चाओं को देखते हुए, मुझे लगता है कि निम्नलिखित दिशानिर्देशों को निर्धारित करना आवश्यक है: –
(i) यदि किसी आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के मामले में रिमांड के आदेश सहित कोई मजिस्ट्रियल कार्रवाई/आदेश पारित करने की आवश्यकता है। जो एक ऐसे अपराध के लिए दर्ज किया गया है जो पहले से ही परिसीमन से वर्जित है, अभियुक्त को अवसर का नोटिस देने के बाद, परिसीमा/माफी की अवधि के विस्तार के बारे में स्पष्ट आदेश पारित किए बिना न्यायालय ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगा।
(ii) अभियुक्त को केवल तभी रिमांड पर भेजा जाएगा जब न्यायालय सकारात्मक रूप से परिसीमा के विस्तार या देरी को माफ करने पर विचार करता है और अभियुक्त को रिमांड पर देने के लिए आधार के साथ मामला अच्छी तरह से स्थापित है।
(iii) यदि न्यायालय सीमा बढ़ाने या देरी को माफ करने के लिए अनुकूल आदेश देने का विकल्प नहीं चुनता है, तो अभियुक्त को रिमांड पर नहीं भेजा जाएगा और उसे तुरंत रिहा कर दिया जाना चाहिए।
(iv) यदि पहले से ही परिसीमा द्वारा वर्जित अपराध के लिए दर्ज मामले पर कोई मजिस्ट्रियल कार्रवाई/आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आरोप पत्र दायर किया गया है, तो न्यायालय को परिसीमा की अवधि बढ़ाने और माफ करने के लिए आदेश पारित करना होगा। अभियुक्त को अवसर का नोटिस देने के बाद उसमें दर्ज कारणों से और न्याय के हित में देरी या विस्तार को अस्वीकार करना। मजिस्ट्रेट के समक्ष चार्जशीट का संज्ञान लेने के लिए उपरोक्त आदेश पारित किया जाएगा।
(v) धारा 473 Cr.P.C के तहत अभियोजन द्वारा दायर किसी भी याचिका के अभाव में भी विस्तार / क्षमा या सीमा की अस्वीकृति के आदेश आवश्यक हैं।
(vi) यदि न्यायालय समय वर्जित अपराध के लिए दायर चार्जशीट का संज्ञान लेता है, बिना किसी सीमा की अवधि को बढ़ाने या देरी को माफ करने के लिए कोई आदेश पारित किए बिना, अभियुक्त को उसे रिहा करने के लिए याचिका दायर करने का अधिकार होगा, भले ही वह कुछ भी हो। कार्यवाही का चरण, सीमा के आधार पर।
(vii) यदि एफ.आई.आर. के समय अपराध परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं है। दर्ज किया गया था, लेकिन जांच के दौरान सीमा समाप्त हो गई, आरोप पत्र धारा 473 Cr.P.C के तहत एक उचित आवेदन के साथ दायर किया जाना है। इस तरह के आवेदन दायर होने की स्थिति में, न्यायालय अभियुक्त को अवसर का नोटिस देगा और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित करेगा। यदि देरी को मौखिक आदेश के माध्यम से क्षमा किया जाता है तो ही चार्जशीट पर संज्ञान लिया जा सकता है।
(viii) यदि बाहरी कारणों से चार्जशीट को धारा 473 Cr.P.C के तहत दायर याचिका के बिना फाइल पर लिया गया है। ऊपर बताए अनुसार दाखिल चार्जशीट के साथ और देरी को माफ करने के आदेश के बिना, अभियोजन पक्ष धारा 473 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर कर सकता है। कार्यवाही के किसी बाद के चरण में भी, किन्हीं स्वीकार्य कारणों से।
हालाँकि, उक्त याचिका पर एक आदेश अभियुक्त को अवसर की सूचना दिए जाने के बाद ही पारित किया जा सकता है। धारा 473 Cr.P.C के तहत दायर ऐसी याचिका पर सकारात्मक आदेश। न्याय के हित में बताए गए कारणों की वास्तविकता और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद यह एक नियमित नहीं हो सकता है।
(ix) यदि एफ.आई.आर. के समय अपराध परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं है। दर्ज किया गया था और जब आरोप पत्र दायर किया गया था, लेकिन न्यायालय की ओर से संज्ञान लेने में देरी के कारण सीमा समाप्त हो गई, अदालत धारा 473 सीआरपीसी के तहत किसी भी याचिका के लिए जोर नहीं देगी, लेकिन आरोप का संज्ञान लेगी शीट, अपने स्वयं के विलंब के कारणों को दर्ज करके।
स्पष्टता के लिए, खंडपीठ ने पैरा 64 में स्पष्ट किया है कि, “चूंकि दूसरे प्रतिवादी ने संज्ञान के आदेश को रद्द करने के लिए एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की है, ताकि अभियोजन पक्ष धारा 473 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर कर सके। पी.सी. चार्जशीट के साथ और यह लंबित है, इस आपराधिक मूल याचिका को उपरोक्त अवलोकन के साथ निपटाया जाता है,”।
“आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में पारित आदेशों के आधार पर, याचिकाकर्ता धारा 473 Cr.P.C के तहत प्रथम प्रतिवादी द्वारा दायर की गई किसी भी याचिका की स्थिति में अपनी आपत्तियां उठा सकता है। यहां तक कि अगर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका लंबित है, लेकिन स्थगन का कोई आदेश नहीं है, तो याचिकाकर्ता को चार्जशीट को रद्द करने के लिए एक नई आपराधिक मूल याचिका दायर करने या परिसीमा के आधार पर उसे रिहा करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर करने की स्वतंत्रता होगी। . नतीजतन, संबंधित विविध याचिका बंद की जाती है।”
अंत में, खंडपीठ ने पैरा 65 पर मजबूती से पकड़ रखते हुए निष्कर्ष निकाला कि, “अलग होने से पहले, यह न्यायालय इस मामले को आदेशों के लिए सुरक्षित रखने के बाद हुए एक बदसूरत मोड़ के बारे में रिकॉर्ड में रखता है। इस याचिका में इस अदालत को आदेश पारित करने से रोकने के लिए छद्म नाम से धमकी भरे पत्र भेजे गए थे। भेजने वाले का इस तरह का ओछा रवैया केवल कायरता और अदालत की प्रक्रिया के प्रति उपेक्षा को प्रदर्शित करेगा।”
“अदालतें इस तरह की धमकियों के लिए अनुकूल नहीं हैं और वे सस्ते प्रयास न्याय प्रदान करने के रास्ते में नहीं खड़े होंगे। इस क्रिमिनल ओरिजिनल पिटीशन में आदेश पारित करके उपरोक्त संदेश को जोरदार शब्दों में दिया गया है।
संक्षेप में, हम इस प्रकार देखते हैं कि यह एक बहुत ही उल्लेखनीय मामला है जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में सीमा अवधि बढ़ाने के लिए पर्याप्त विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
इस प्रकार यह कोई पुनरावृत्ति नहीं है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने इस प्रमुख मामले में बहुत ही सुंदर ढंग से, वाक्पटुता और प्रभावी ढंग से जो कुछ भी निर्धारित किया है, उस पर सभी अदालतों को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। इससे इनकार नहीं!