भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रामू अप्पा महापात्र बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025 INSC 147) मामले में यह स्पष्ट किया है कि आपराधिक मामलों में अदालतों को अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्तियों (Extra-Judicial Confessions) का मूल्यांकन किस प्रकार करना चाहिए। यह मामला क्रिमिनल अपील नंबर 608/2013 से उत्पन्न हुआ, जिसमें सेशंस कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दोषसिद्धि को चुनौती दी गई थी। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी ठहराया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता और मृतका मांडा एक लिव-इन रिलेशनशिप में थे। अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता द्वारा किए गए कथित अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्तियों को दोषसिद्धि के प्रमुख आधार के रूप में प्रस्तुत किया। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने इन स्वीकारोक्तियों को पर्याप्त प्रमाण मानते हुए दोषसिद्धि को बरकरार रखा। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इन स्वीकारोक्तियों की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता की गहन समीक्षा की और यह निष्कर्ष निकाला कि संदेह, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, संदेह से परे प्रमाण (Proof Beyond Reasonable Doubt) का स्थान नहीं ले सकता।
निर्णय का सारांश
न्यायमूर्ति अभय एस. ठीक और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने अपने निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्तियों के प्रमाणिकता की जांच की और पाया कि:
- अभियुक्त के विरुद्ध प्रमुख साक्ष्य केवल उन गवाहों के बयान थे जिन्होंने दावा किया कि अपीलकर्ता ने मांडा को पीसने वाले पत्थर और लकड़ी के डंडे से मारने की बात स्वीकार की।
- कोई प्रत्यक्ष भौतिक प्रमाण (जैसे, अभियुक्त के कपड़ों पर रक्त के धब्बे, हथियारों पर फॉरेंसिक मिलान) नहीं मिला जिससे उसकी संलिप्तता प्रमाणित हो।
- कुछ गवाहों ने स्वयं माना कि अपीलकर्ता “भ्रमित मानसिक स्थिति” में था और उनके बयान पुलिस के समक्ष दिए गए मूल बयानों से भिन्न थे।
- अभियोजन पक्ष के साक्ष्य परस्पर विरोधाभासी और अपूर्ण पाए गए, जिससे स्वीकारोक्तियों की प्रमाणिकता संदेह के घेरे में आ गई।
न्यायालय ने इन विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता की सजा को निरस्त कर दिया और उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया जब तक कि किसी अन्य लंबित मामले में उसकी आवश्यकता न हो।
विधिक विश्लेषण
पूर्ववर्ती निर्णयों का संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में राजस्थान राज्य बनाम राजा राम (2003) 8 SCC 180, संसार चंद बनाम राजस्थान राज्य (2010) 10 SCC 604, और सहदेवन बनाम तमिलनाडु राज्य (2012) 6 SCC 403 मामलों का हवाला दिया। इन निर्णयों में स्थापित किया गया कि:
- अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्तियां स्वभावतः कमजोर प्रमाण होते हैं, और इनकी गहन जांच आवश्यक होती है।
- ये स्वीकारोक्तियां स्वेच्छा से, मानसिक संतुलन में, और स्वतंत्र साक्ष्यों से पुष्ट होनी चाहिए।
- न्यायालयों को चाहिए कि वे अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्तियों को तभी स्वीकार करें जब अन्य साक्ष्य उन्हें पूर्णतः विश्वसनीय सिद्ध करें।
कानूनी तर्क: सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य श्रृंखला की अपर्याप्तता को मुख्य आधार बनाते हुए निर्णय दिया:
- अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति की स्वाभाविक दुर्बलता:
- अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान परस्पर विरोधी थे।
- कुछ गवाहों के अनुसार, अभियुक्त मानसिक रूप से भ्रमित था, जिससे स्वैच्छिकता और सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है।
- साक्ष्य का अभाव:
- अभियोजन पक्ष कोई ठोस भौतिक प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहा।
- कथित हत्या के हथियार या अभियुक्त के कपड़ों पर कोई पुष्टि करने योग्य रक्त के धब्बे नहीं मिले।
- गवाहों के विरोधाभासी बयान:
- पुलिस के समक्ष दर्ज धारा 161 सीआरपीसी के बयान और अदालत में दिए गए गवाही में महत्वपूर्ण अंतर थे।
- प्राकृतिक आचरण में असमानता:
- मृतका के भाई और मकान मालिक की प्रतिक्रिया अस्वाभाविक लगी, जिससे यह संकेत मिला कि स्वीकारोक्तियों को अत्यधिक महत्व देना तर्कसंगत नहीं है।
इन तथ्यों के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियोजन पक्ष अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा।
न्यायिक प्रभाव और भविष्य की राह
यह निर्णय न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह पुष्टि करता है कि न्यायालयों को अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्तियों पर अत्यधिक निर्भर नहीं होना चाहिए।
- अभियोजन पक्ष को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि किसी मामले में अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति प्रस्तुत की जाती है, तो वह अन्य स्वतंत्र और ठोस साक्ष्यों से पुष्ट हो।
- रक्षा वकील इस निर्णय का उपयोग उन मामलों में कर सकते हैं जहां केवल स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही हो।
- यह फैसला संदेह से परे प्रमाण (Proof Beyond Reasonable Doubt) के सिद्धांत को मजबूत करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई निर्दोष व्यक्ति गलत तरीके से दोषसिद्ध न हो।
महत्वपूर्ण कानूनी अवधारणाओं की व्याख्या
- अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति:
- ये वे स्वीकारोक्तियां होती हैं जो न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं दी जातीं।
- न्यायालय इन्हें प्रमाण के रूप में तभी स्वीकार करता है जब ये स्वतंत्र रूप से पुष्ट हो।
- धारा 161 सीआरपीसी बयान:
- ये वे बयान होते हैं जो पुलिस द्वारा जाँच के दौरान दर्ज किए जाते हैं।
- यदि गवाह बाद में इससे भिन्न बयान देता है, तो उसकी गवाही की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।
- परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला:
- आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि के लिए सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्य आपस में जुड़कर निर्विवाद निष्कर्ष तक पहुंचने चाहिए।
- यदि एक भी कड़ी कमजोर है, तो आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।
निष्कर्ष
रामू अप्पा महापात्र बनाम महाराष्ट्र राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्धि नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने यह दोहराया कि:
- हर पहलू को संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए।
- स्वीकारोक्तियां तभी मान्य होंगी जब वे ठोस साक्ष्यों से पुष्ट हों।
- मात्र संदेह को प्रमाण का स्थान नहीं दिया जा सकता।
इस निर्णय का प्रभाव भविष्य के मुकदमों पर पड़ेगा, जिससे अपराध न्याय प्रणाली अधिक न्यायसंगत और साक्ष्य-आधारित बन सकेगी।





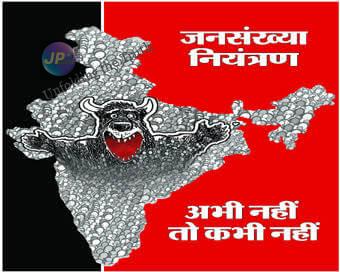








Leave a Reply