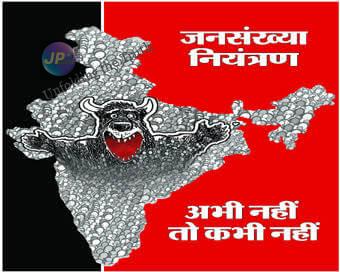सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए कई न्यायिक निर्णयों के पश्चात् पुनः अनुच्छेद 142 की सार्थकता का मुद्दा उभर आया-
भारत के सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए जी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की बेंच ने भारतीय संविधान Indian Constitution के अनुच्छेद 142 Article 142 का हवाला देते हुए यह आदेश पारित किया। शीर्ष अदालत का कहना था कि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा प्राप्त उक्त अधिकारों का इस्तेमाल यहाँ उचित है।
क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142?
संविधान के अनुच्छेद 142 की उपधारा 1 कहती है कि, “उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो।”
संविधान का यह प्रावधान देश की शीर्ष अदालत को खास मामलों में “पूर्ण न्याय” करने का व्यापक अधिकार देता है।
संविधान में इस अनुच्छेद को शामिल करने की आवश्यकता को संविधान सभा की बहस से समझा जा सकता है। इस अनुच्छेद पर बहस के दौरान श्री ठाकुर दास भार्गव ने इसकी जरूरत को दर्शाते हुए कहा था कि प्राकृतिक न्याय NATURAL JUSTICE सभी कानून से ऊपर है, और सर्वोच्च न्यायालय भी कानून से ऊपर रहना चाहिये ताकि उसे कोई भी आदेश पारित करने का पूरा अधिकार हो जिसे वह न्यायसंगत मानता है।
संविधान का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है और लगभग असीमित अधिकार देता है। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय “पूर्ण न्याय” ‘COMPLETE JUSTICE’ के लिए इन शक्तियों का उपयोग करने के लिए अधिकृत है और कोई भी नियम या कानून, कार्यकारी अभ्यास या कार्यकारी परिपत्र या विनियम आदि के प्रावधान उसे उपयुक्त न्याय करने में बाधा नहीं बन सकते हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय, हर अर्थ में, कानून से ऊपर होगा।
संविधान के अनुच्छेद 142 का दायरा-
अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्तियां व्यापक हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों के द्वारा इसके दायरे और सीमा को परिभाषित किया है।
इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मामलों और लैंडमार्क केसेस निम्न है-
- ‘प्रेम चंद गर्ग बनाम आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद’ (1962);
- ‘ए.आर. अंतुले बनाम आर.एस. नायक और अन्य’ (1988);
- ‘यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ’ (1991);
- ‘सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ’ (1998)
सर्व प्रथम, प्रेम चंद गर्ग बनाम एक्साइज कमिश्नर उत्तर प्रदेश 1962 में, बहुमत की राय से अनुच्छेद 142 (1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की। अदालत ने इस मामले में कहा कि पूर्ण न्याय करने के लिए यह अदालत जो भी आदेश देगी, वो न केवल संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के अनुरूप होने चाहिएं, बल्कि प्रासंगिक वैधानिक कानूनों के मूल प्रावधानों के साथ असंगत भी नहीं होने चाहिएं।”
यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1991 में, गैस के खराब रखरखाव के कारण भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया प्लांट से हानिकारक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव होने के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए अदालत ने भारत सरकार को पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने और उनके सर्वोत्तम हितों की रक्षा करने के लिए अधिकृत किया।
मुआवजे के रूप में कंपनी को 470 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश देते हुए, खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142(1) के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे पर कुछ गलतफहमियों को दूर करना आवश्यक है। अदालत ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश देने के लिए स्वयं को संसदीय कानूनों से ऊपर रखकर ‘पूर्ण न्याय’ ‘COMPLETE JUSTICE’ की प्राप्ति के लिए वैधानिक कानूनों पर लागू प्रतिबंध को अनुच्छेद 142 के दायरे से बाहर रखा।
अदालत ने अपने फैसला में कहा, “सामान्य कानूनों में निहित प्रावधानों पर जिस तरह प्रतिबंध होते हैं, वे अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त संवैधानिक अधिकारों पर लागू नहीं हो सकते हैं …यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त अधिकार व्यक्त सांविधिक निषेध के अधीन हैं। अगर ऐसा होता है, तो इससे यह प्रतीत होगा कि संवैधानिक प्रावधान वैधानिक प्रावधान के अधीन हैं…”
अनुच्छेद 142 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति अदालत को ‘पूर्ण न्याय’ के लिए प्रयास करने का अधिकार देती है। इसके दायरे को लेकर अदालत ने मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रधान सचिव के मामले में विस्तार से चर्चा की थी और समझाने का प्रयास किया था कि सर्वोच्च न्यायालय जनता के व्यापक हित के लिए असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकती है ताकि जनता का कानून के शासन में विश्वास न डगमगाए।
इसी तरह ए.आर. अंतुले बनाम आर.एस. नायक 1988 के मामले में अदालत ने साफ तौर पर समझाया कि अदालत के किसी भी फैसले में उसका न्यायिक विवेक न तो मनमाना होना चाहिए और न ही किसी भी तरह से से निर्धारित वैधानिक कानूनों के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हो सकता है।
ज्ञात हो की संविधान के अनुच्छेद 142 के इसी तथ्य को बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ’ 1998 मामले में भी दोहराया गया| इस मामले में यह कहा गया कि इस अनुच्छेद का उपयोग मौज़ूदा कानून को प्रतिस्थापित करने के लिये नहीं, बल्कि एक विकल्प के तौर पर किया जा सकता है|
ए जी पेरारिवलन के मामले में अनुच्छेद 142 का लिया सहारा-
इसी अधिकार का माकूल उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, “पूर्ण न्याय” के उद्देश्य से राज्यपाल द्वारा पेरारिवलन को क्षमा करने में अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए उसे रिहा करने का फैसला किया।
राज्यपाल ने अनुच्छेद 161, जो राज्यपाल को पेरारिवलन की रिहाई का फैसला करने की अधिकार देता है, के तहत राष्ट्रपति को राज्य के मंत्रिमंडल की सिफारिश भेजने से पहले उसे कई महीनों तक लटकाए रखा।
अनुच्छेद 161 राज्यपाल को किसी भी मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, या सजा में छूट देने या सजा को निलंबित करने या सजा को कम करने अधिकार देता है।
जानकारी हो की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति के फैसले का इंतजार करने के फैसले से असहमत है, वो भी तब जब तमिलनाडु राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी सिफारिश काफी समय पहले ही दे दी है। यह देखते हुए अदालत ने कहा कि “कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।”
अदालत ने इससे पहले पेरारीवलन को उनकी लंबी कैद और पैरोल पर बाहर रहते हुए पैरोल की शर्तों का किसी तरह उल्लंघन न करने और किसी प्रकार की शिकायत का मौका न देने को मद्देनजर रखते हुए उन्हें जमानत दे दी थी।
न्यायिक संयम, न्यायिक हस्तक्षेप की एक संकल्पना है जो न्यायाधीशों को उनकी स्वयं की शक्ति को सीमित करने के लिये प्रेरित करती है| यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीशों को तब तक नियमों में बदलाव नहीं करना चाहिये जब तक वे असंवैधानिक प्रतीत न हो क्योंकि असंवैधानिक कानून स्वयं ही विवाद का विषय बन जाते हैं।