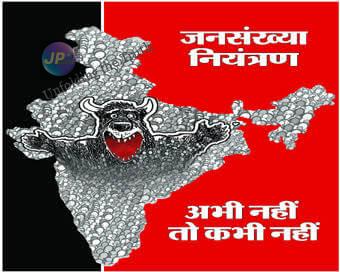सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 (सीआरपीएफ नियम) के नियम 27 को बरकरार रखा, जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा का प्रावधान है।
उड़ीसा उच्च न्यायालय, न्यायालय कटक के उस निर्णय के विरुद्ध केंद्र द्वारा दायर दीवानी अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील को खारिज कर दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश डॉ डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, “आमतौर पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति को सजा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर सेवा नियम इसे जांच के अधीन सजा के रूप में लागू करने की अनुमति देते हैं, तो ऐसा ही हो। बल को कुशल बनाए रखने के लिए, अवांछनीय तत्वों को हटाना आवश्यक है और यह बल पर नियंत्रण का एक पहलू है, जो सीआरपीएफ अधिनियम की धारा 8 के आधार पर केंद्र सरकार के पास बल पर है। इस प्रकार, बल पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, यदि सामान्य नियम-निर्माण शक्ति का प्रयोग करते हुए, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा निर्धारित करते हुए नियम बनाए जाते हैं, तो इसे सीआरपीएफ अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत नहीं माना जा सकता है, खासकर तब जब धारा 11 की उप-धारा (1) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उसमें प्रयोग की जाने वाली शक्ति अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन है।
कोर्ट ने कहा कि इसलिए, हम मानते हैं कि नियम 27 द्वारा निर्धारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा सीआरपीएफ अधिनियम के अंतर्गत आती है और यह लगाए जाने वाले दंडों में से एक है।
बेंच ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति सेवानिवृत्ति लाभों के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित किए बिना कैडर से मृत लकड़ी को हटाने का एक अच्छी तरह से स्वीकृत तरीका है, यदि अन्यथा देय है। यह सेवानिवृत्ति लाभों को प्रभावित किए बिना सेवा को समाप्त करने का एक और रूप है।
संक्षिप्त तथ्य-
प्रतिवादी2 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल3 में हेड कांस्टेबल था। उस पर अपने साथी सहकर्मी पर हमला करने और गाली-गलौज करने के आरोप में आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। आगामी जांच में प्रतिवादी के खिलाफ आरोप सिद्ध पाए गए। इसके परिणामस्वरूप, प्रतिवादी को दिनांक 16.02.2006 के आदेश के तहत अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी ने विभागीय अपील दायर की, जिसे सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक (पी) ने दिनांक 28.07.2006 के आदेश के तहत खारिज कर दिया।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अधिवक्ता आनंद शंकर ने प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व किया। इस मामले में, प्रतिवादी सीआरपीएफ में एक हेड कांस्टेबल था और अपने साथी सहकर्मी पर हमला करने और दुर्व्यवहार करने के आरोपों पर आरोप पत्र दायर किया गया था। आगामी जांच में प्रतिवादी के खिलाफ आरोप सिद्ध पाए गए और इसके परिणामस्वरूप, उसे 2006 में एक आदेश के तहत सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। इससे व्यथित होकर, उसने विभागीय अपील दायर की, जिसे सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक (पी) ने खारिज कर दिया। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश और उसकी अपील खारिज होने का विरोध करते हुए, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर इसे अनुमति दी कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा सीआरपीएफ, 1949 की धारा 11 (1) में निर्दिष्ट दंडों में से एक नहीं थी। व्यथित होने के कारण, एकल न्यायाधीश के आदेश को अपीलकर्ताओं ने डिवीजन बेंच के समक्ष अपील के माध्यम से प्राथमिकता दी। बेंच ने इसमें कोई योग्यता नहीं पाई और इसे खारिज कर दिया।
इसलिए, अपीलकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
मामले के उपरोक्त संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “आमतौर पर सेवा में किसी व्यक्ति को सेवा के अनुबंध या ऐसी सेवा को नियंत्रित करने वाले कानून में निर्दिष्ट दंड नहीं दिया जा सकता है। दंड या तो सेवा अनुबंध में या अधिनियम में या ऐसी सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। … इसलिए हमारे विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या धारा 11 सीआरपीएफ अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले छोटे दंडों के संबंध में संपूर्ण है या यह केवल अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा पूरक एक ढाँचा प्रदान करता है।
न्यायालय ने कहा कि सीआरपीएफ अधिनियम, 1949 को अधिनियमित करते समय विधायी इरादा यह घोषित करना नहीं था कि केवल वही छोटे दंड लगाए जा सकते हैं जो सीआरपीएफ अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट हैं, बल्कि, अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को खुला छोड़ दिया गया था और लगाए जाने वाले दंड अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अधीन थे।
इसने कहा “…यदि सीआरपीएफ अधिनियम में बल पर नियंत्रण केंद्र सरकार को सौंपने की परिकल्पना की गई है और धारा 11 के तहत लगाए जाने वाले विभिन्न दंड अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अधीन हैं, तो केंद्र सरकार अपने सामान्य नियम-निर्माण शक्ति का प्रयोग करते हुए, बल पर पूर्ण और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, उस धारा में निर्दिष्ट दंडों के अलावा अन्य दंड निर्धारित कर सकती है, जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड भी शामिल है”।
इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि दी गई सजा साबित कदाचार के लिए चौंकाने वाली अनुपातहीन नहीं है, बल्कि, उसकी पिछली सेवा को देखते हुए, मामले में पहले से ही सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है और प्रतिवादी को और अधिक छूट नहीं दी जानी चाहिए, जो एक अनुशासित बल का हिस्सा था और अपने सहयोगी पर हमला करने का दोषी पाया गया है।
“परिणामस्वरूप, हमें प्रतिवादी को दी गई सजा में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा कारण नहीं मिला”, इसने निष्कर्ष निकाला।
तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया, उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादी को दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा की पुष्टि की।
वाद शीर्षक – भारत संघ और अन्य बनाम संतोष कुमार तिवारी